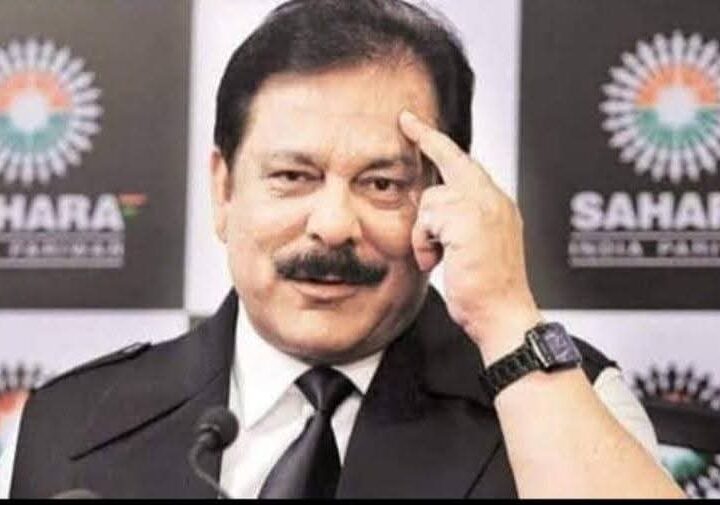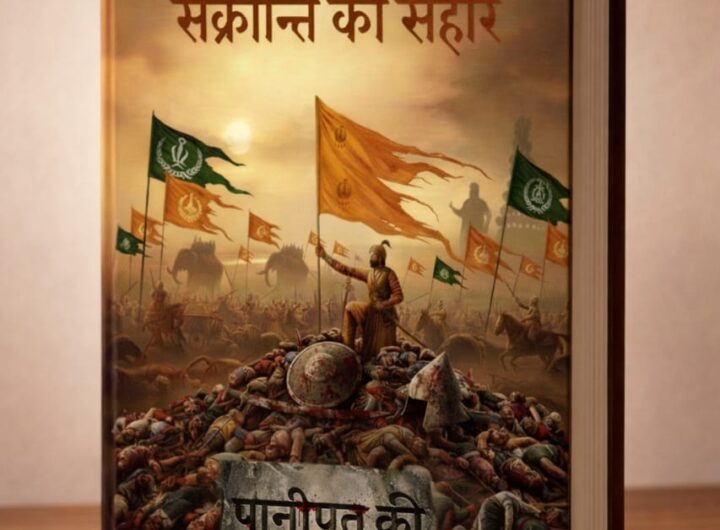झपकी की संस्कृति: भारत की आंगनवाड़ी और बाल विकास की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समझ
शिक्षा केवल जानकारी का हस्तांतरण नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन और संवेदनशीलता की शिक्षा है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में ‘झपकी’ या ‘नेप टाइम’ जैसी सरल लगने वाली अवधारणाएं, असल में मनोवैज्ञानिक पुनर्भरण, भावनात्मक संरक्षण, और सामाजिक तालमेल के गहरे साधन होते हैं।
जहाँ 1950 के दशक के अमेरिका में ‘नेप टाइम’ एक सुसंगठित, संवेदी और सांस्कृतिक शैक्षिक अभ्यास था, वहीं भारत की आंगनवाड़ी प्रणाली में यह पहलू अब भी एक ‘परछाईं’ की तरह उपस्थित है — अनुभव में मौजूद, पर नीति और संरचना में अस्पष्ट।
भारत की आंगनवाड़ी प्रणाली: एक सामाजिक आवश्यकता
भारत की आंगनवाड़ी (Anganwadi) प्रणाली 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के अंतर्गत प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य था:
* 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
* किशोरियों और माताओं को पोषण संबंधी परामर्श
* समुदाय के भीतर बाल विकास के प्रति जागरूकता
लेकिन प्रश्न है — क्या यह प्रणाली ‘बाल मनोविज्ञान’ और ‘भावनात्मक स्थिरता’ जैसी गहराइयों तक पहुँच पा रही है?
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: विश्राम का स्थान कहां है?
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में नींद और विश्राम की महत्वपूर्ण भूमिका है:
1. स्मृति का समेकन (Memory consolidation) : झपकी के दौरान मस्तिष्क सीखी गई जानकारी को स्थायी स्मृति में बदलता है।
2. भावनात्मक नियमन (Emotion regulation) : अपर्याप्त नींद बच्चों में चिड़चिड़ापन, आक्रोश और सामाजिक पलायन को जन्म देती है।
3. ध्यान और ग्रहणशीलता : विश्राम के बाद बच्चा अधिक सक्रिय, एकाग्र और ग्रहणशील होता है।
परंतु अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों में:
* न तो कोई समर्पित ‘नेप टाइम’ निर्धारित है,
* न विश्राम के लिए उपयुक्त वातावरण,
* न कार्यकर्ताओं के पास इसके महत्व की मनोवैज्ञानिक समझ।
ऐसे में बच्चा केवल थका हुआ शरीर नहीं, भावनात्मक रूप से उपेक्षित मन भी बनता है।
सामाजिक दृष्टिकोण: झपकी एक सांस्कृतिक संकेतक
भारत जैसे विविध सामाजिक ढांचे में ‘झपकी’ कई मायनों में सांस्कृतिक व्यवहार है:
* ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर की नींद सामूहिक जीवनचर्या का हिस्सा रही है।
* परंपरागत समाजों में दादी-नानी की कहानियाँ झपकी के समय जुड़ी होती थीं।
* लेकिन जब शिक्षा संस्थान इस व्यवहार को ‘समय की बर्बादी’ या ‘अनुत्पादकता’ से जोड़ते हैं, तब संवेदनशीलता पर दक्षता हावी हो जाती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं समाज के हाशिए से आती हैं, जिनपर पोषण, टीकाकरण, सर्वेक्षण, रिपोर्टिंग आदि का इतना बोझ होता है कि बच्चों के भावनात्मक अधिकारों के लिए उनके पास समय, संसाधन और प्रशिक्षण — तीनों का अभाव है।
तुलनात्मक अंतर्दृष्टि: अमेरिका और फिनलैंड के उदाहरण
अमेरिका (1950s) : किंडरगार्टन में ‘नेप टाइम’ एक शैक्षिक अवधारणा थी, जहाँ संगीत, मंद रोशनी और शिक्षिका की मातृत्वपूर्ण भूमिका बच्चों को सुरक्षा और शांति देती थी।
फिनलैंड (वर्तमान में) : यहां बच्चों को ‘रिस्टॉयतुमिसहेत्की’ (आराम का समय) के दौरान झपकी लेने या शांत गतिविधियों में संलग्न होने की स्वतंत्रता दी जाती है। झपकी एक अधिकार की तरह संरक्षित है — भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक तैयारी के लिए।
भारत (वर्तमान में) : आंगनवाड़ी में झपकी का कोई औपचारिक शैक्षिक स्थान नहीं है। यह कार्यकर्ता की सुविधा और केंद्र की भीड़ पर निर्भर होता है। परिणामस्वरूप यह सामाजिक रूप से मान्य लेकिन संस्थागत रूप से अनुपस्थित व्यवहार बन गया है।
* नीति, प्रशिक्षण और संवेदना की ज़रूरत
‘नेप टाइम’ जैसे छोटे-से अभ्यास में भारत की प्रारंभिक बाल शिक्षा की बड़ी कमियाँ दिखाई देती हैं:
* नीति में विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य को स्थान देना होगा।
* आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा कि भावनात्मक पोषण भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक।
* और सबसे बढ़कर, शिक्षा को समाज की लय और बच्चों की नाज़ुकता के साथ जोड़ना होगा।
भारत को चाहिए कि वह बाल शिक्षा में संवेगात्मक देखभाल, धीमेपन, और पुनर्भरण को अधिकार के रूप में माने — न कि केवल एक “बैकअप विकल्प”।
* झपकी — एक विराम नहीं, एक संभावना
यदि हम चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा न केवल शिक्षित, बल्कि संतुलित, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बने — तो हमें ‘झपकी’ जैसे प्रतीकों को केवल नींद नहीं, मूल अधिकार की दृष्टि से देखना होगा।