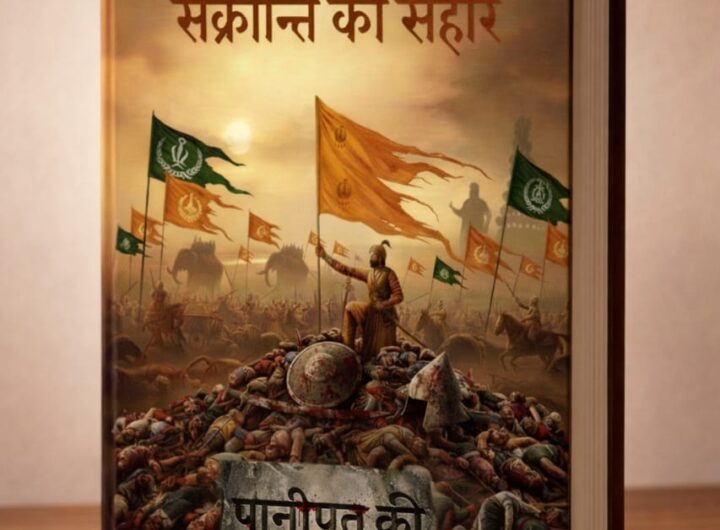प्रोफेसर डॉ. लोपा मेहता,
जो मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रहीं,
एनाटॉमी डिपार्टमेंट की हेड थीं ।
उन्होंने 78 साल की उम्र में Living Will बनाया,
जब शरीर जवाब देने लगे और लौटने की कोई गुंजाइश न बचे,
तब इलाज नहीं किया जाए।
न वेंटिलेटर,
न ट्यूब,
न अस्पताल में बेवजह की दौड़।
वो चाहती हैं कि आख़िरी वक़्त शांति से बीते,
जहाँ इलाज की ज़िद नहीं, समझदारी हो।
डॉ. लोपा ने केवल ये दस्तावेज़ नहीं लिखा,
एक शोध-पत्र भी प्रकाशित किया है ,
जिसमें मृत्यु को एक स्वाभाविक,
समय-निर्धारित,
जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया।
उनका कहना है कि आधुनिक चिकित्सा मृत्यु को कभी स्वतंत्र रूप में देख ही नहीं पाई।
वो मानती रही कि मौत हमेशा किसी बीमारी की वजह से होती है, और अगर बीमारी का इलाज हो जाए तो मौत टाली जा सकती है। लेकिन शरीर का विज्ञान इससे कहीं ज़्यादा गहरा है।
उनका तर्क है ,
शरीर कोई अनंत चलने वाला यंत्र नहीं है।
यह एक सीमित प्रणाली है,
जिसमें एक निश्चित जीवन-ऊर्जा होती है।
यह ऊर्जा हमें किसी टंकी से नहीं,
बल्कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिलती है।
वही सूक्ष्म शरीर जिसे अनुभव तो हर कोई करता है,
पर देखा नहीं जा सकता ,मन, बुद्धि, स्मृति, और चेतना ,इन्हीं से मिलकर बना है यह सिस्टम ।
यह सूक्ष्म शरीर एक माध्यम है,
जिससे जीवन-शक्ति आती है और पूरे शरीर में फैलती है।
यही शक्ति शरीर को जीवित रखती है।
यह नाड़ी, धड़कन, पाचन और सोचने की क्षमता ,सब कुछ उसी के भरोसे चलता है।
लेकिन यह शक्ति अनंत नहीं है।
हर शरीर में इसकी एक निश्चित मात्रा होती है।
जैसे किसी मशीन में फिक्स बैटरी हो ,
न ज़्यादा हो सकती है न कम।
जितनी चाभी भरी राम ने उतना चले खिलौना टाइप ।
डॉ. लोपा लिखती हैं कि जब शरीर में मौजूद इस ऊर्जा का अंतिम अंश खर्च हो जाता है,
तो सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है।
यही वो क्षण होता है, जब देह स्थिर हो जाती है,
और हम कहते हैं,
“प्राण निकल गया।”
यह प्रक्रिया न बीमारी से जुड़ी है,
न किसी चूक से।
यह शरीर की अपनी आंतरिक गति है,
जो गर्भ में ही शुरू हो जाती है,
और जब पूरी हो जाती है,
तब मृत्यु होती है।
इस ऊर्जा का व्यय हर पल होता रहता है एक-एक कोशिका,
एक-एक अंग, धीरे-धीरे अपने जीवन की लंबाई पूरी करते हैं।
और जब संपूर्ण शरीर का कोटा खत्म होता है,
तब शरीर शांत हो जाता है।
मौत का समय कोई घड़ी से नापा गया क्षण नहीं होता।
यह एक जैविक समय है ,हर व्यक्ति के लिए अलग। किसी का जीवन 35 साल में पूरा होता है, किसी का 90 में।
लेकिन दोनों ही अपनी पूरी इकाई जीते हैं।
कोई अधूरा नहीं मरता,
अगर हम उसे मजबूरी या हार न कहें।
डॉ. लोपा ने अपने लेख में ये भी कहा है कि आधुनिक चिकित्सा जब मृत्यु को टालने की जिद करती है,
तो वो केवल शरीर नहीं,
पूरे परिवार को थका देती है।
ICU में महीने भर की साँसें कभी कभी वर्षों की कमाई ले जाती हैं।
रिश्तेदार कहते रह जाते हैं “अभी उम्मीद है”,
पर मरीज की देह कब की कह चुकी होती है “बस अब बहुत हो गया।”
इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जब मेरा समय आए,
तो बस KEM ले जाना।
जहाँ मुझे भरोसा है कि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा। इलाज के नाम पर खिंचाई नहीं की जाएगी।
मेरे शरीर को रोका नहीं जाएगा जाने दिया जाएगा।
अब सवाल ये है ,
क्या हम सबने अपने लिए ऐसा कुछ सोचा है?
क्या हमारा परिवार उस इच्छा का सम्मान करेगा?
क्या इच्छा का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पा सकेगा?
क्या हमारे देश के अस्पतालों में ऐसी इच्छाओं की इज्जत बची है,
या अब भी हर सांस पर बिल बनेगा,
और हर मौत पर आरोप?
सब इतना आसान नहीं लगता है,
तर्क और इमोशन का मैनेजमेंट शायद सबसे कठिन कामों मेव सेवक है ।
अगर मौत को एक नियत,
शांत और शरीर के भीतर से तय प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करें,
तो शायद मौत से डर भी कम हो,
और डॉक्टर से उम्मीद भी थोड़ी सच्ची हो।
मुझे लगता है मौत से लड़ना बंद करना चाहिए,
उससे पहले जीने की तैयारी करनी चाहिए ।
और जब वो आए ,तो शांति से, गरिमा से उसे जाने देना चाहिए ।
बुद्ध की भाषा में मौत एक प्रमोशन है ।
लेकिन क्या मेरी ख़ुद की ये सोच 70 के बाद रह पायेगी?
हम खुद ही नहीं जानते ।